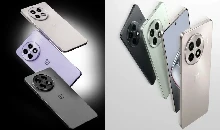बच्चे दिव्यांगता से नहीं दूसरों के व्यवहार से ज्यादा परेशान होते हैं

जितने परेशान बच्चे अपनी दिव्यांगता से नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा दूसरों के व्यवहार से होते हैं। स्कूल और शिक्षा में हर टीचर व घटक एक समान नहीं होते। एक विचारधारा के नहीं होते। इसलिए कहीं न कहीं बेहतर की उम्मीद हमेशा रहती है।
शिक्षा की कई सारी कहानियां हैं। इनमें से कुछ कहानियां समय समय पर फिल्मों में देखने को मिलती रही हैं। हिचकी हमारी शैक्षिक कहानियों में से एक है। यह फिल्म दरअसल हमारी शिक्षा में समावेशीकरण और बहिष्करण के विभिन्न पहलुओं को विमर्श पटल पर गहरे तक उभारती है। बात सिर्फ फिल्म की ही नहीं है बल्कि हमारी शिक्षा ऐसे दिव्यांग बच्चों के साथ किस प्रकार का बरताव करती है उस ओर भी शिद्दत से विमर्श करती है। छुटपन में बच्ची को स्कूलों से इसलिए निकाल बाहर किया गया क्योंकि वो बोलते बोलते हिचकी लेती है। चक चक करती है आदि आदि। उस पात्र को स्कूल से यह कहते हुए निकाला जाता है कि हम इसे क्यों निकाल रहे हैं उस वज़ह को हम नहीं बताएंगे। अंत में वह बच्ची न केवल स्कूलों से निकाल बाहर की जाती है बल्कि कक्षा में भी उसे अपने सहपाठी और शिक्षक की डांट और उपहास का पात्र बनना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हमारी शिक्षा समावेशीकरण के सिद्धांत को तवज्जो देती है। इसी शैक्षिक दर्शन को मानते हुए विभिन्न निजी स्कूलों में मोटी फीस लेकर बच्चों को कहीं न कहीं आत्मकुंठा और बहिष्करण की मार झेलनी पड़ती है।
जिद देखिए कि किसी तरह यदि दिव्यांग बच्चे स्कूल पार कर लेते हैं तब उन्हें निजी जीवन में भी दोयम दर्ज़े के बरताव से गुज़रना पड़ता है। यहां तक कि माता−पिता और अभिभावक अपने ही ऐसे बच्चों के व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए भी देखे जाते हैं। तुर्रा यह कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 को इस लचर तरीके से इस फिल्म में और फिल्म के बाहर भी इस्तमाल किया जाता है जिससे एक संदेश स्पष्ट तौर पर समाज में फैलता है कि इस कानून में ही कोई खामी है जो सामाजिक और आर्थिक तौर से पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें सामान्य और मुख्यधारा के स्कूलों में दाखिला देना ज़ायज नहीं है। यह कहीं न कहीं सामान्य बच्चों के साथ न्याय नहीं है। जबकि इस तर्क का दूसरा पहलू यह है कि यही वह कानून है जो समावेशी शिक्षा और सब के लिए समान शिक्षा की वकालत तकरीबन सौ सालों से कर रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कानून बनने में सौ साल का लंबा संघर्षपूर्ण वर्ष रहा है। लेकिन आज भी विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट और अध्ययन बताते हैं कि आज भी शिक्षा की मुख्यधारा से तकरीबन सात करोड़ बच्चे कटे हुए हैं। गौरतलब है कि हमने 1990 में थाईलैंड के जोमिटियन शहर में वैश्विक मंच पर घोषणा की थी कि 2000 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा मुहैया करा देंगे। लेकिन 2000 का सहस्राब्दि लक्ष्य भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। वर्ष 2000 में डकार के सम्मेलन में यह लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा 2015 रखी गयी थी। वह भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। 2016 में वैश्विक मंच ने दुबारा सतत् विकास लक्ष्य में शामिल प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए 2030 का लक्ष्य तय किया है।
हिचकी दरअसल हमारी शिक्षा में गहरे पैठ चुकी हिचकी की ओर हमारे नागर समाज का ध्यान खींचती है। जहां विभिन्न स्कूलों से संबंध रखने वाले टीचर, प्रिन्सिपल और अभिभावक हैं। उनकी मानें तो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा मुख्यधारा के स्कूलों में नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए अलग से स्कूल और टीचर की व्यवस्था की जाए। इससे कक्षा में शिक्षण और समाजिकरण में दिक्कतें आती हैं। जो इस फिल्म में बच्ची को न केवल साथ पढ़ने वाले दोस्तों की बल्कि कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर की विभेदीकरण के रवैए से परेशान है। जितने परेशान हमारे बच्चे अपनी दिव्यांगता से नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा दूसरों के व्यवहार से होते हैं। स्कूल और शिक्षा में हर टीचर व घटक एक समान नहीं होते। एक विचारधारा के नहीं होते। इसलिए कहीं न कहीं बेहतर की उम्मीद हमेशा रहती है। जो इस फिल्म में भी उभर कर आती है। खान साहब तय करते हैं। कहने कि बजाए पूछने और सवाल करने के दर्शन में विश्वास करते हैं। और बच्ची से पूछते हैं तुम क्या चाहती हो? बजाए कि खान साहब अपनी राय थोपते। संवाद करने और प्रश्न करने की संस्कृति वह फलक मुहैया कराती है जहां समावेशी शिक्षा की प्रकृति संरक्षित है। और तय होता है कि बच्ची को विशेष न लिया जाए। उसके साथ भी सामान्य बच्चों की तरह बरताव किया जाए।
आज हमारे बच्चे परीक्षा में फेल नहीं होते बल्कि वे शिक्षा की वर्गीय विभाजन और मूल्यांकन के पैरामीटर पर पिछड़ जाते हैं। हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की अपनी क्षमता और समझ होती है। हमें बच्चों की क्षमता और समाज तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जांचने परखने की तकनीक और विधि को मांजना होगा। इस फिल्म में पेरेंट्स टीचर मीट में एक ओर मुख्यधारा के बच्चों के पेरेंट्स आते हैं वहीं जो आरटीई के दबाव में 9वीं एफ के बच्चे हैं उस कक्षा में न तो बच्चे आते हैं और न उनके अभिभावक। टीचर निराश होती है। लेकिन सहकर्मी ने चलते चलते जो बात कही वह एक रोशनदान की तरह है जहां हमें बच्चों की दुनिया को देखने और समझने की आवश्यकता है। उस टीचर ने कहा जब आप कक्षा मैदान में लेती हैं तो आपको तो पीटीएम भी मैदान या उनके घर में करनी चाहिए। यह एक प्रस्थान बिंदु है जहां टीचर को बात जंच जाती है और बच्चों के घरों की ओर लौटती है। जहां पंचर ठीक करते, ताश खेलते, डेंटिंग पेंटिंग करते बच्चे नज़र आते हैं। जहां उसकी मुलाकात अभिभावकों और उनके सपनों से होती है। यहीं से उसकी टीचिंग एप्रोच में भी बदलाव घटित होता है। वह बच्चों के आप जीवन में घटने वाली घटनाओं, वस्तुओं के ज़रिए पढ़ाने की बज़ाए ऑब्जर्वेशन की ओर ध्यान दिलाती है। मसलन पंचर लगाने, ताश के खेल से गणित पढ़ाने आदि के सिद्धांतों को व्यवहार में घटा कर बच्चों को समझाने का प्रयास करती है।
जब एक टीचर लीक से हर कर कुछ करने की कोशिश करता है तब ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां उसके माकूल होती हैं। क्या स्कूल, क्या परिवार, क्या समकर्मी सब के सब विपरीत हो जाते हैं। तोड़ने और पछाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। दरअसल उसमें उनका भी कोई खास दोष नहीं है। क्योंकि उन्होंने कभी नई राह बनाने की कोशिश ही नहीं की। जो करिकूलम, स्लेबस, टेक्स्ट बुक मिल गईं उन्हें पूरा कराने और साल के अंत में परीक्षा की भट्ठी में झोंकने में अपनी जिम्मेदारी का अंत मान लेते हैं। यह एक न टूटने वाली कड़ी है खासकर टीचिंग प्रोफेशन में। एक तो टीचिंग को बाई च्वाइस अपनाने वाले कम होते हैं, जो अपनाते हैं उन्हें टींचिंग में कोई ज़्यादा मजा नहीं आता। यदि वे अपने व्यवसाय को जीने लगें। चुनौती की तरह लेने लगें तो काफी समस्या कम हो जाएगी। दरअसल शिक्षा के मायने भी बदले हैं। यदि सिर्फ परीक्षा पास करना मायने है तो बच्चे लाखों की संख्या में परीक्षा पास कर अच्छे अंकों की टोकरी सिर पर उठाए जब जॉब में आते हैं तब उन्हें अंक और अनुभव, जीवन की समझ और पुस्तकीय लिखित सूत्रों के बीच एक फांक नज़र आता है। प्रोफेशनल्स मानते हैं कि इधर के कुछ सालों से जो बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं उनके पास डिग्री तो है लेकिन अपने विषय की समझ नहीं है। उन्हें समझाना और उनसे काम लेना बहुत कठिन होता है। इन बच्चों में आत्मस्वाभिमान इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें नई चीज सीखने से महरूम कर देती है।
वर्तमान शिक्षा की हिचकी को बड़े परदे पर जिस प्रतिबद्धता से समावेशी, बहिष्करण की प्रक्रिया को दिखाया गया है वह हमारे लिए आंखें खोलने वाली है। बच्चे कसूरवार नहीं होते। बच्चे सिर्फ बच्चे होते हैं। उन्हें हम अपनी सहूलीयत के लिए विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ हम कैसे पेश आएं। क्या हम उन्हें सुनाने के लिए हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं या वे जो कहना चाहते हैं उसके लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। बच्चों में सवाल करने और अपनी बात को रखने के लिए उकसा रहे हैं या हम जो कहना चाहते हैं उसे वे चुपचाप सुन लें।
पाव्लो फ्रेरे ने उत्पीड़ितों के शिक्षाशास्त्र में जिक्र किया है कि कक्षा में चुप्पी की संस्कृति सबसे ज़्यादा घातक है। यदि बच्चे सवाल नहीं करते, यदि बच्चे तर्क नहीं करते तो वह कक्षा व शिक्षा कैसी होगी इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। जबकि इस फिल्म में लगातार समांतर चलने वाली कक्षा 9वीं एफ में बच्चों को अपनी सृजनात्मकता को उभारने और बोलने की पूरी छूट है। अपने परिवेश से सीखने और वस्तुओं के प्रयोग करने में यह बच्चों की मदद करता है। नवाचार की भी ज़मीन मिलती है जहां बच्चे अवसर पाते ही अपनी क्षमता और प्रकृतिप्रदत्त समझ का प्रयोग नेशनल साइंस फेयर में करते हैं। अंत में स्कूल और टीचर से बहिष्कृत बच्चे मुख्यधारा के बच्चों के समक्ष एक मिसाल के तौर पर उभरते हैं। इस विश्वास के साथ कि यदि शिक्षा में समुचित और समावेशी अवसर मुहैया कराया जाए और शिक्षकीय मागदर्शन मिले तो हर बच्चा आम से खास हो सकता है।
-कौशलेंद्र प्रपन्न
अन्य न्यूज़