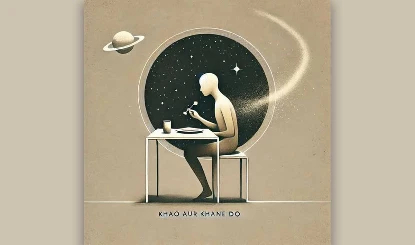
ज़िंदगी की एक फिलॉसफी है—जियो और जीने दो। जीने के लिए खाना ज़रूरी है, तो कहना चाहिए, "खाओ और खाने दो।" तभी तो हम जी पाएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। लेकिन जब बात आती है इस फिलॉसफी के उलट—"ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा" जैसे नारों की, तब लोकतंत्र की नींद हराम हो जाती है। भला बिना खाए काम कैसे चलेगा, और जिंदा कैसे रहेंगे?
हमारे एक दोस्त हैं, जो बस खाने के लिए ही जीते हैं। कॉलेज के समय की बात है। मेस में लंच टाइम उनके बैठने के बाद ही शुरू होता। खाना शुरू करते तो यह सुनिश्चित करते कि आख़िरी टाइम तक सभी को खिलाकर ही खुद खाना खत्म करें।
खुद का खाना खत्म करने के बाद, वे दूसरों की प्लेट को ऐसे घूरते, मानो उसमें छुपा कोई खज़ाना खोज रहे हों। आखिरकार, कोई न कोई अपनी प्लेट उठाकर उसमें चावल और बची-खुची दाल डाल देता। इस 'दान' को लेकर वे सीधे रूम की ओर प्रस्थान करते, जहां आराम से खाते। ऐसा लगता, जैसे दिन का आधा समय वे इस महायज्ञ में लगा देते थे।
मेस वर्कर्स ने एक बार तो हड़ताल ही कर दी। उनका कहना था, "जब तक इन्हें मेस में एंट्री दी जाएगी, खाना नहीं बनेगा।" आखिरकार, उन्होंने मेस में आना बंद कर दिया और प्लेट रूम पर ही मंगाने लगे।
बाकी बचा समय वे शाम के खाने की चिंता में बिताते। "शाम को क्या बनेगा?" "कहीं मेस बंद तो नहीं हो जाएगी?" अगर ऐसा लगता कि मेस बंद हो सकती है, तो तुरंत किसी शादी या पार्टी में 'अनाधिकृत प्रवेश' का जुगाड़ लगाने में जुट जाते। ये 'खाद्य-समाज' के सुपरहीरो थे, जिनका एक ही मकसद था—खाने के सभी अवसरों को भुनाना।
आदमी को भगवान ने बनाया ही खाने के लिए है। जानवर तो बस पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन आदमी का असली "भोजन" तो पेट भरने के बाद शुरू होता है। जानवर जहाँ अपने खाने के प्रति बड़े संवेदनशील और स्पष्ट होते हैं—अब गधे को घास के बजाय चिकन परोसोगे तो क्या वह खाएगा? शेर को मांस की जगह घास खिलाने लगे तो वह खिलाने वाले से ही अपनी भूख शांत करेगा।
वहीं इंसान ऐसा पतित प्राणी है, जो सब कुछ खा सकता है। घर की दाल छोड़कर अगर बाहर की मुर्गी मिले, तो सबसे पहले उस पर लपकेगा। वह किसी का हक, किसी के सपने, नौकरियाँ, राहत सामग्री, बजट, रिश्वत, यहाँ तक कि गरीब की आत्मा तक निगल सकता है। ज़रूरत हो तो वह सब कुछ खा सकता है—देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से। जड़-चेतन, मूर्त-अमूर्त, हर चीज़।
आम आदमी ज़मीन पर बैठकर खाता है, नेता कुर्सी पर। और कुर्सी पर बैठते ही नेताजी की भूख सर्वव्यापी, सार्वकालिक और सर्वग्राही हो जाती है। नेताओं के लिए "खाओ और खाने दो" का सिद्धांत विभागों को खुला लाइसेंस देता है—"खाओ, जितना खा सकते हो। सात पीढ़ियों तक के लिए खा जाओ।" पुल, सड़क, बाँध, इमारतें, आयोग भवन, सीमेंट, बालू, कागज के नोट, सोना-चांदी, अंगारे, भूवर—ये सब खाने की वस्तुएँ हैं। आदमी है कि सब कुछ पचा सकता है। पशुओं का चारा, गैस, डीज़ल, पशुआहार—हर चीज़ भोजन बन सकती है।
संस्थाएँ भी तो खाने के लिए हैं। सेवा रूपी तलवार से डोनेशन की फसल काटी जा रही है।
कोई खाकर बौरा रहा है, कोई गुर्रा रहा है। कोई नहीं खाकर भी सुर्खियों में आ रहा है। फूल-मालाओं से लदा... वो अखबार में जगह घेर रहा है, लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। खा सभी रहे हैं, लेकिन खाने को तो हमारे धर्मग्रंथों में भी मान्यता दी गई है—"भूखे पेट भजन न होय गोपाला।"
असली खिलाड़ी तो वही है जो खाकर पचा ले। यह तो नेता और अधिकारियों के बस की ही बात है, जो स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनैतिकता की त्रिफला चूर्ण की मदद से जो भी खाते हैं, सब पचा जाते हैं। उस पर अगर सत्ता का अभयदान भी मिल जाए, तो अपच होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकारें खजाना इसलिए खाती हैं ताकि उसे दुबारा भरा जा सके। अगर सरकार का खजाना भरा रहेगा, तो जनता टैक्स देना भूल जाएगी।
सब चिढ़ते हैं उनसे जो खाते नहीं, अनशन पर बैठ जाते हैं। वो नहीं खाते, तो खाने वालों की नींद हराम हो जाती है।
दो ही तरह के लोग हैं—खाने वाले, जिन्हें खाने को मिलता है, और न खाने वाले, जिन्हें खाने का अवसर नहीं मिलता। अगर उचित खाने को मिले, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खाने से इनकार करे। लोग कसम खा रहे हैं... कोई किसी का माथा खा रहा है, कोई किसी का वक्त। जो कहता है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है, वो झूठी कसम खा रहा है।
एक जादूगर खेल दिखा रहा था... कांच की ट्यूब लाइटें, गिलास—सब गपागप खा रहा था। यह देख मुझे हंसी आई। अरे, यह कौन सा जादू है? यह तो हमारे नेता बरसों से करते आ रहे हैं। वो खाने पर आयें तो पुल ,सड़क,चारा यहाँ तक की पुब्लिक टॉयलेट्स तक खा जाएँ । मुफ्त में जादू दिखा रहे हैं और जनता ताली पीट रही है।
नेता खाते ही नहीं... खिलाते भी हैं—झूठे वायदे, खोखली घोषणाएँ, मुफ्त की रेवड़ियाँ, ताकि जनता बदले में वोट रूपी फसल दे। फिर नेता लोग उस फसल को काटते हैं और उसे दिल्ली की मंडी में उचित दाम पर बेचते हैं। अगर उनकी अपनी पार्टी उचित दाम नहीं लगाती, तो विरोधी पार्टियों से दाम लगवाते हैं। इस फसल के बदले में कुर्सी मिलती है, पद मिलते हैं, और अधिकार मिलते हैं।
कई बार इतना खा लिया जाता है कि पचना मुश्किल हो जाता है, और सड़न की दुर्गंध फैलने लगती है। विरोधी पार्टियाँ इसे सूंघ लेती हैं। उन्हें खाने से परहेज नहीं होता, लेकिन मौका न मिलने का गुस्सा बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता है।
जाँच आयोग खाने की जाँच करते हैं, टेस्ट सैंपल लिए जाते हैं, और रिपोर्ट सबको बराबरी से कहने का हक दिलाती है।
जाँच की तलवार से, रिश्वत की तलवार से बस धन, पद और प्रतिष्ठा की फसल काटी जा रही है। जनता को सिर्फ सात्विक, सफेद धन ही खाने की इजाजत है। काला धन जैसा गरिष्ठ भोजन सिर्फ नेता लोग ही पचा सकते हैं।
देश इसी खाने की बीमारी से "खाता-पीता देश" कहलाता है। अगर नेता और अधिकारी खाना छोड़ दें, तो अनजाने में ही कई जिंदगियाँ भूख से मर जाएँगी। पुलिस, कोर्ट-कचहरी सब ठप हो जाएँगे, और ट्रैफिक चौराहों पर पुलिसवाले आराम से बैठ जाएँगे।
प्रकृति खाना नहीं खाती, उसका स्वभाव देने का है—हवा, जल, आकाश, अग्नि। हमने प्रकृति का सब कुछ खा लिया। जंगल खा लिए, तो इमारतें बनीं; सड़कें खा लीं, तो गड्ढे बने; नदियाँ खाईं, तो नल-कूप बने।
देश की इस "खाऊ संस्कृति" में कुछ लोग तो इतने विशेषज्ञ हो गए हैं कि देश में कोई भी कानून, नियम, आवंटन या स्कीम लागू हो, इससे पहले ही यह तय कर लेते हैं कि उसे खाने का तरीका क्या होगा। राजनीति में आए नए लोग पहले तो थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन पाकर जल्द ही वो भी "खाऊ वीर" बन जाते हैं। अब चाहे वो शहर के बजट का हिस्सा हो, स्कूल की जमीन, या फिर किसी सरकारी योजना का अनुदान—सब कुछ उनकी भोजन की थाली में सज जाता है।
भ्रष्टाचार से भरी ज़िंदगी पर "लोकप्रियता" का लेप है। यह "खाओ और खाने दो" का दर्शन बन चुका है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मिठास बन गया है, जो ऊपर से नीचे तक सबको घोल-घोल कर पिला दिया गया है।
"खाने की कला" एक सनातनी प्रथा है, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं। और सच में, यही कला विशुद्ध भारतीय धरोहर है, जो "विकसित" और "समृद्ध" लोकतंत्र के चारों स्तंभों को मजबूती दे रही है।
तो साहब, खाइए! बस इतना ध्यान रहे कि अगले चुनाव तक पचा भी लीजिए, वरना बदहजमी की गैस से कुर्सी भी तो हिल ही सकती है।
- डॉ. मुकेश असीमित